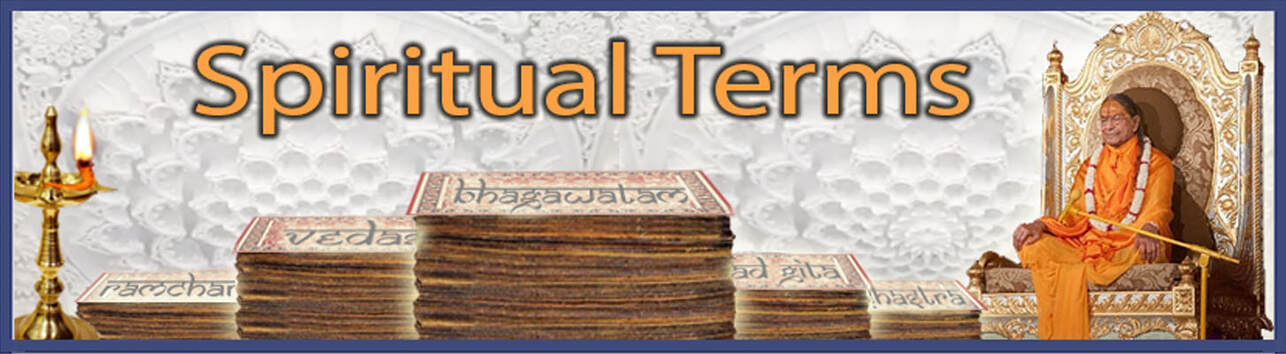वास्तविकता की अक्षुण्ण अनुभूति ही वास्तविक ज्ञान है। इसी प्रकार ईश्वर का दृढ़ ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है।
ईश्वरीय ज्ञान के दो भाग हैं पहला सत् का ज्ञान तथा दूसरा असत् का ज्ञान। इन दोनों ज्ञान के होने से मायिक संसार से वैराग्य होता है। यह मायिक संसार ब्रह्मलोक तक है।
ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति को ज्ञान मार्ग कहते हैं । ज्ञान मार्ग पर "ए बी सी" सीखने से पहले साधन-चतुष्टय सम्पन्न होना अनिवार्य है अर्थात निम्नलिखित चार लक्षण मन में हों ।
ईश्वरीय ज्ञान के दो भाग हैं पहला सत् का ज्ञान तथा दूसरा असत् का ज्ञान। इन दोनों ज्ञान के होने से मायिक संसार से वैराग्य होता है। यह मायिक संसार ब्रह्मलोक तक है।
ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति को ज्ञान मार्ग कहते हैं । ज्ञान मार्ग पर "ए बी सी" सीखने से पहले साधन-चतुष्टय सम्पन्न होना अनिवार्य है अर्थात निम्नलिखित चार लक्षण मन में हों ।
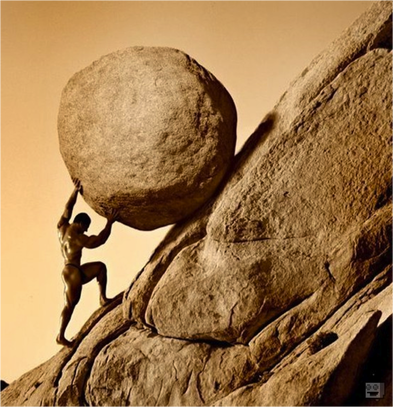 Seemingly impossible six states of mind are prerequisites for stepping on the path of Gyan
Seemingly impossible six states of mind are prerequisites for stepping on the path of Gyan
ज्ञान मार्ग की प्रवेशिका में दाखिला पाने के लिए अंतःकरण इन चार अवस्थाओं से सम्पन्न होनी चाहिए। इन चारों को प्राप्त अंतः करण को साधन-चतुष्टय-संपन्न (साधन चतुष्टय सिद्धि) कहा जाता है।
- नित्यनित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते - नित्य तथा अनित्य वस्तुओं के परिज्ञान ।
- इहामुत्रफलभोग परित्यागः - जीव सुख पाने की अभिलाषा से वस्तुओं में अनुराग करता है।नित्य तथा अनित्य वस्तुओं के ज्ञान से साधक के अंतःकरण से संसार की कामना स्वतः ही निकल जाएगी । क्योंकि जब संसार स्वयं ही एक दिन समाप्त हो जाएगा तो संसार का सुख सनातन कैसे हो सकता है ?
- शमादि षट संपत्ति: - मन के छह गुणों की सिद्धि।
- शम - मन पर पूर्ण नियंत्रण और फिर उसे ईश्वर की ओर ले जाना।
- दम - इंद्रियों पर नियंत्रण।
- तितिक्षा - इस अटल समझ के कारण धैर्य और सहनशीलता रखना कि हर अच्छा या बुरा भाग्य अपने ही कर्मों का फल है, जिसे भोगना ही पड़ता है।
- श्रद्धा - ईश्वर में अटूट विश्वास।
- समाधान – सभी संदेह दूर हो गए हैं और ईश्वर प्राप्ति की अवधारणा में स्पष्टता है।
- उपरति - संसार से पूरी तरह वैराग्य और फिर मुक्ति की इतनी प्रबल इच्छा किस साधक कुछ भी करने के लिए तत्पर रहे । यह ज्ञान मार्ग की प्रवेशिका में जाने के लिए मन की ऐसी स्थिति होनी चाहिए ।
- मुमुक्षत्वमितिस्फुटम् - मुक्ति की अदम्य इच्छा।
उपरोक्त मानसिक अवस्थाओं को प्राप्त कर लेने के उपरांत व्यक्ति को वैराग्य का अभ्यास करना पड़ता है [1]। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु तथा व्यक्ति के प्रति न राग हो न द्वेष हो।
फिर वह ज्ञान के अन्य स्तरों को पार करता है
वास्तव में ये सभी स्तर वैराग्य की प्रगति हैं। अंततः साधक माया के एक पहलू पर विजय प्राप्त करता है। माया के दो पहलू हैं
- विवेक - नश्वर व नित्य वस्तुओं में भेद करने की क्षमता, और इस प्रकार विशेष रूप से शाश्वत नित्य प्राप्त करने के लिये ही प्रयत्न करना
- वैराग्य - संसार से पूर्ण वैराग्य । इस स्थिति में यदि एकाएक पत्नी, पुत्र, धन, व्यापार, सब कुछ एक साथ हानि हो जाए तो भी साधक का मन विचलित नहीं होगा।
- शमादि षट् संपत्ति – ऊपर बताए गए मन के छह गुण।
- मुमुक्षुत्व - मुक्ति की तीव्र इच्छा।
- श्रवण – मुक्ति प्राप्ति के लिए तत्त्वज्ञान को सुनना।
- मनन - दर्शन पर गहराई से विचार करना।
- निदिध्यासन – निष्ठापूर्वक शिक्षाओं का पालन करना।
- समाधि – ध्यान में तल्लीन हो जाना ।
वास्तव में ये सभी स्तर वैराग्य की प्रगति हैं। अंततः साधक माया के एक पहलू पर विजय प्राप्त करता है। माया के दो पहलू हैं
स्वरूपावरिका माया के 2 रूप
- राजस गुण और
- तामस गुण - आसुरी प्रवृत्तियों
गुणावरिका माया सत्व गुणी माया है
स्वरूपावरिका माया जीव के असली रूप को भुला देती है । "मैं" आत्मा हैं जो अमर और दिव्य है, फिर भी, जीव स्वरूपावरिका माया के कारण इस वास्तविकता को सदा से भूला हुआ है । ज्ञानी स्वरूपावरिका माया को जीत लेता है अर्थात जीव स्वयं (आत्मा) का ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञात रहे - ये गुण जाते नहीं हैं पर दब जाते हैं । फिर भी, तीसरा सत्वगुण अभी भी हावी है ।
गीता कहती है,
गीता कहती है,
सत्त्वाद् संजायते ज्ञानम्
"आत्मा का ज्ञान सत्व गुण से उत्पन्न होता है"।
आत्मा के ज्ञान से इतना आनंद मिलता है कि ज्ञानी समझता है कि उसने वास्तव में भगवत्प्राप्ति का आनंद प्राप्त कर लिया है। ज्ञानी की इस अवस्था को ब्रह्मभूतावस्था कहा जाता है, वह स्तर जहाँ वह आत्मा के ज्ञान के आनंद के अलावा कुछ भी नहीं जानता या महसूस करता है। ऐसे ज्ञानी के लिए गीता कहती है
आत्मा के ज्ञान से इतना आनंद मिलता है कि ज्ञानी समझता है कि उसने वास्तव में भगवत्प्राप्ति का आनंद प्राप्त कर लिया है। ज्ञानी की इस अवस्था को ब्रह्मभूतावस्था कहा जाता है, वह स्तर जहाँ वह आत्मा के ज्ञान के आनंद के अलावा कुछ भी नहीं जानता या महसूस करता है। ऐसे ज्ञानी के लिए गीता कहती है
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेषुभूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ गीता १८.५४
"इस अवस्था में ज्ञानी सदा हर्षित रहता है। न तो वह दुखी होता है और न ही उसे किसी चीज की इच्छा होती है"। वह हर किसी में और हर जगह आत्मा को महसूस करता है। अतः वह पूर्णतः निष्पक्ष हो जाता है।
लेकिन उसने अभी निराकार ब्रह्म [3] को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए इस अवस्था से पतन अभी भी संभव है। तो, आत्म-ज्ञान की स्थिति तक पहुँच चुके ज्ञानी आगे क्या करते हैं?
लेकिन उसने अभी निराकार ब्रह्म [3] को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए इस अवस्था से पतन अभी भी संभव है। तो, आत्म-ज्ञान की स्थिति तक पहुँच चुके ज्ञानी आगे क्या करते हैं?
भक्ति के अतिरिक्त और किसी साधन से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए माया से मुक्ति के लिए भक्ति अनिवार्य है। जैसा कि जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं -
मोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरियसी॥ शंकराचार्य
जगद्गुरु शंकराचार्य का दावा है कि श्री कृष्ण भक्ति के बिना शम या मन की शुद्धि भी संभव नहीं है, तो यह स्पष्ट है कि मुक्ति अप्राप्य है;
शुद्धयति हि नान्तरात्मा कृष्णपदाम्भोजभक्तिमृते ॥ शंकराचार्य
लेकिन, भक्ति दो प्रकार की होती है, क्योंकि एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दो रूप हैं। वेद कहते हैं;
द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे, मूर्तं चैवामूर्तं च।
ईश्वर के दो रूप हैं; एक साकार ब्रह्म और दूसरा रूप निर्गुण निराकार ब्रह्म। जगद्गुरु शंकराचार्य भी निम्नलिखित शब्दों में यही कहते हैं;
मूर्तं चैवामूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। इत्युपनिष्त्तयोर्वा द्वौभक्तौभगवदुपदिष्टौ॥
ज्ञानी निराकार ब्रह्म की भक्ति करता है। ज्ञानी ध्यान को केंद्रित करने के लिये ब्रह्म को प्रकाश के बिंदु के रूप में मान कर उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि भक्त भगवान के रूपों में से एक को अपने इष्ट के रूप में चुनता है, भगवान के उस दिव्य रूप को सभी दिव्य गुणों से संपन्न करता है [6] और फिर उस दिव्य रूप का ध्यान करता है। इस प्रकार, दोनों भगवान के प्रति समर्पित हैं। ज्ञानी निराकार भगवान की पूजा करते हैं और भक्त अपनी पसंद के एक विशेष रूप से भगवान की पूजा करते हैं [7]।
तो जब दोनों भगवान की पूजा करते हैं तो किस रास्ते पर चलना आसान है?
तो जब दोनों भगवान की पूजा करते हैं तो किस रास्ते पर चलना आसान है?
भक्ति मार्ग की तुलना में ज्ञान मार्ग अधिक कठिन है। ज्ञानमार्ग का साधक ईश्वर के किसी भी नाम, रूप, लीला और गुणों का आश्रय नहीं ले सकता, इसलिए चंचल मन को किसी भी वस्तु पर केन्द्रित करना अत्यंत कठिन है।
|
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया॥ कठोपनिषत्
"ज्ञान मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है"।
ग्यान अगम प्रत्युह अनेका। साधन कठिन न मन महुँ टेका॥
ज्ञान कै पंथ कृपाण कै धारा। परेत खगेस होहिं नहिं बारा॥ राम चरित मानस "ज्ञान मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। ज्ञान मार्ग की साधना भी बड़ी कठिन है"।
|
लेकिन यदि कोई ज्ञान मार्ग पर चलने की पूर्व योग्यता को पूरा कर ले और सभी कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करे तो भी ज्ञान के मार्ग पर और भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि,
1. जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं;
1. जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं;
क्लेषोऽधिकतरस्तेषा मव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवऔयते॥ गीता १२.५
"मनुष्य का शरीर साकार है इसलिए उनके लिए निराकार ब्रह्म के अदृष्ट, अव्यवहार्य व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल है"।
2. इस रास्ते पर पहला कदम उठाने की योग्यता बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। जैसा कि मैंने इस लेख में पहले बताया है, इस मार्ग पर कदम रखने से पहले चार गुणों में महारत हासिल करनी होती है, जिसे साधन चतुष्टय कहा जाता है।
निर्विणणानां ज्ञानयोगः॥
"सांसारिक आसक्ति समाप्त किये बिना कोई ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकता।"
विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगुणशालिनः। मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासा योग्यता मता॥ शंकरा.
"सबसे पहले, पूर्ण अनासक्ति अत्यंत कठिन है। फिर अन्य मानसिक स्थितियाँ और भी जटिल हैं"।
भक्ति मार्ग से इसकी तुलना करने पर, जो न तो पूरी तरह से विरक्त हैं और न ही संसार में आसक्त हैं, वे भक्ति के मार्ग पर चलने के पात्र हैं।
भक्ति मार्ग से इसकी तुलना करने पर, जो न तो पूरी तरह से विरक्त हैं और न ही संसार में आसक्त हैं, वे भक्ति के मार्ग पर चलने के पात्र हैं।
नातिसक्तो न वैराग्यभागस्यामधिकार्यसौ॥ भ. र.सिं.
सर्वेधिकारिणो ह्यत्र हरिभक्तौ यथ नृप॥ पदम पुराण
शास्त्रतः श्रूयते भक्तौ नृमात्रस्याधिकारिता ॥ भ. र.सिं.
भगवत्प्राप्त्युपायो हि सर्वसाधन हीनता॥ रामानंद
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न जप तप मख उपवासा॥ रा.च.मानस
सर्वेधिकारिणो ह्यत्र हरिभक्तौ यथ नृप॥ पदम पुराण
शास्त्रतः श्रूयते भक्तौ नृमात्रस्याधिकारिता ॥ भ. र.सिं.
भगवत्प्राप्त्युपायो हि सर्वसाधन हीनता॥ रामानंद
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न जप तप मख उपवासा॥ रा.च.मानस
तुलसी दास के अनुसार "भक्ति के मार्ग पर चलने में क्या कठिनाई है। मन को वश में करने के लिए योगाभ्यास नहीं करते, तपस्या करते हैं, विस्तृत वैदिक विधान करते हैं"।
3. यदि कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तो उसके पग-पग पर पतन की संभावना बनी रहती है क्योंकि ज्ञानी अपने ज्ञान और वैराग्य पर निर्भर रहता है [1] , और भगवान का सहारा नहीं लेता है। इसके विपरीत, एक भक्त पूरी तरह से भगवान की कृपा पर और भगवान पर पूर्ण निर्भर होता है। भागवत निम्नलिखित श्लोक में यही कहता है:
येऽन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्ध बुद्धयः ।
"आत्म-साक्षात्कार होने पर, ज्ञानी अपने आप को मुक्त मान सकता है, लेकिन वह अभी भी माया के दायरे से बाहर नहीं हुआ है। वह फिर से वहाँ से पतन हो सकता है"।
आरुह्यकृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदंघ्र्यः॥ भाग. १०.२.३३
"ज्ञान के उच्च स्तर को प्राप्त करने के बाद भी ज्ञानी पूर्ण पतन का होता है"। लेकिन भक्त, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहते हुए, कभी नहीं गिरते। बल्कि आपके द्वारा रक्षित होने के कारण वे बिना किसी परवाह के मुक्त विचरते हैं
तथा न ते माधव तावकाः क्वचिद् भ्रश्यंति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः।
त्वयभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानी कपमूर्धसु प्रभो॥ भाग. १०.२.३३
त्वयभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानी कपमूर्धसु प्रभो॥ भाग. १०.२.३३
कुछ लोगों को चुनौती अच्छी लगती है तो कुछ लोग आसान राह पकड़ लेते हैं... कई बाधाओं को पार कर ज्ञानी भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है।
तो गंतव्य पर पहुँचने के बाद क्या ज्ञानी और भक्त में कोई अन्तर है?
तो गंतव्य पर पहुँचने के बाद क्या ज्ञानी और भक्त में कोई अन्तर है?
ज्ञानी का लक्ष्य भक्त से अलग नहीं है। दोनों एक ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं [4], क्योंकि ईश्वर एक है ।
इसलिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है
इसलिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता: || गीता 12.4
"... अपनी इंद्रियों को संयमित करके और सर्वत्र समचित्त होकर, ऐसे व्यक्ति भी सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं ..."
वास्तव में सबसे बड़ा अंतर लक्ष्य प्राप्त करने के बाद शुरू होता है।
ज्ञानी ईश्वर के साकार रूप में विश्वास ही नहीं करता है और केवल मायिक पीड़ाओं से मुक्ति चाहता है। तो सिद्धि होने पर ज्ञानी को प्राप्त होता है
इस प्रकार, ज्ञानी का ब्रह्म के साथ एकत्व हो जाता है, ब्रह्म आनंद का सागर है। अब त्रिपुटी समाप्त हो गई, फिर ज्ञानी उस आनंद को कैसे भोग सकता है? यदि आप स्वयं ही मिठाई बन जायें, तो आप उस मिठाई का स्वाद कैसे चखेंगे?
परात्पर ब्रह्म के साकार रूप (4) के आनंद की मधुरिमा अकथनीय और नित्य वर्धमान है। कई महान ईश्वर-प्राप्त ज्ञानी पृथ्वी पर परमहंस के रूप में रहते थे। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति हमेशा ब्रह्मानन्द में लीन रहता है और उसे इस संसार का कोई आभास नहीं होता है। वे ब्रह्म के साकार रूप के आनंद का अनुभव मात्र एक इंद्रिय (दृष्टि, श्रवण, स्वाद, स्पर्श, गंध) से करने पर ही निहाल हो गये । ब्रह्म के साकार रूप के सौरस्य ने उनकी समाधि भंग कर दी, और स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रेमानंद के दिव्य सागर में डुबो दिया। उदाहरण के लिए,
उन सभी के पास केवल एक ही इन्द्रिय का विषय था और उन्होंने ऐसे असाधारण दिव्य आनंद का अनुभव किया कि वे अपने पारलौकिक ध्यान के बारे में भूल गए। ऐसा है भगवान के साकार रूप का आनंद।
ज्ञानी, जो भगवान के अमूर्त रूप की पूजा करता है और मुक्ति प्राप्त करता है और जीव शरीर, मन या इंद्रियों के बिना निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जिससे व्यक्ति प्रेम का आनंद प्राप्त करने का अवसर खो देता है क्योंकि निराकार ब्रह्म का कोई रूप, नाम या लीला नहीं है।
वास्तव में सबसे बड़ा अंतर लक्ष्य प्राप्त करने के बाद शुरू होता है।
ज्ञानी ईश्वर के साकार रूप में विश्वास ही नहीं करता है और केवल मायिक पीड़ाओं से मुक्ति चाहता है। तो सिद्धि होने पर ज्ञानी को प्राप्त होता है
- माया और जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्ति।
- दिव्य आत्मा, इंद्रियों, मन या बुद्धि के बिना, शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए निराकार बह्म में लय ।
इस प्रकार, ज्ञानी का ब्रह्म के साथ एकत्व हो जाता है, ब्रह्म आनंद का सागर है। अब त्रिपुटी समाप्त हो गई, फिर ज्ञानी उस आनंद को कैसे भोग सकता है? यदि आप स्वयं ही मिठाई बन जायें, तो आप उस मिठाई का स्वाद कैसे चखेंगे?
परात्पर ब्रह्म के साकार रूप (4) के आनंद की मधुरिमा अकथनीय और नित्य वर्धमान है। कई महान ईश्वर-प्राप्त ज्ञानी पृथ्वी पर परमहंस के रूप में रहते थे। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति हमेशा ब्रह्मानन्द में लीन रहता है और उसे इस संसार का कोई आभास नहीं होता है। वे ब्रह्म के साकार रूप के आनंद का अनुभव मात्र एक इंद्रिय (दृष्टि, श्रवण, स्वाद, स्पर्श, गंध) से करने पर ही निहाल हो गये । ब्रह्म के साकार रूप के सौरस्य ने उनकी समाधि भंग कर दी, और स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रेमानंद के दिव्य सागर में डुबो दिया। उदाहरण के लिए,
- सतयुग के सबसे बड़े ज्ञानी 4 कुमारों ने एक बार हवा के माध्यम से एक अज्ञात सुगंध का अनुभव किया। जिस क्षण उन्होंने सुगंध सूँघी और वे अपने पारलौकिक ध्यान के बारे में भूल गए। इतना ही नहीं वे यह जानने के लिए बेचैन हो गए कि यह कहां से आया है। उनकी समाधि के माध्यम से, उन्हें पता चला कि दिव्य सुगंध एक तुलसी के पत्ते से है जिसे महाविष्णु के चरण कमलों पर रखा गया है। उनके चरणों के स्पर्श से ही सुगंध दिव्य और परम आनंदमय हो गई थी। उन्होंने सोचा, 'यदि तुलसी के पत्ते का आनंद, जो उनके चरणों को छूता है, इतना रमणीय है, तो उनके चरण कमलों के बारे में क्या कहा जा सकता है!' 3) जहाँ तक वे जानते थे कि यह सर्वोच्च आनंद था, और उनसे हमेशा के लिए अपने चरण कमलों में निवास करने का वरदान माँगा। (भागवत 3.15.43 और 3.15.49)।
- इसी तरह, त्रेता युग में, राजा जनक ने श्री राम को सिर्फ एक बार देखा और अपनी बेटी, माता सीता के भव्य विवाह समारोह के बारे में जागरूकता सहित अपने आस-पास की हर चीज के बारे में होश खो बैठे।
- द्वापर युग में श्रीमद्भागवत के वक्ता शुकदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के साकार ब्रह्म का केवल एक गुण सुना था और निराकार ब्रह्म का ध्यान करने में उनकी रुचि समाप्त हो गई थी।
उन सभी के पास केवल एक ही इन्द्रिय का विषय था और उन्होंने ऐसे असाधारण दिव्य आनंद का अनुभव किया कि वे अपने पारलौकिक ध्यान के बारे में भूल गए। ऐसा है भगवान के साकार रूप का आनंद।
ज्ञानी, जो भगवान के अमूर्त रूप की पूजा करता है और मुक्ति प्राप्त करता है और जीव शरीर, मन या इंद्रियों के बिना निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जिससे व्यक्ति प्रेम का आनंद प्राप्त करने का अवसर खो देता है क्योंकि निराकार ब्रह्म का कोई रूप, नाम या लीला नहीं है।