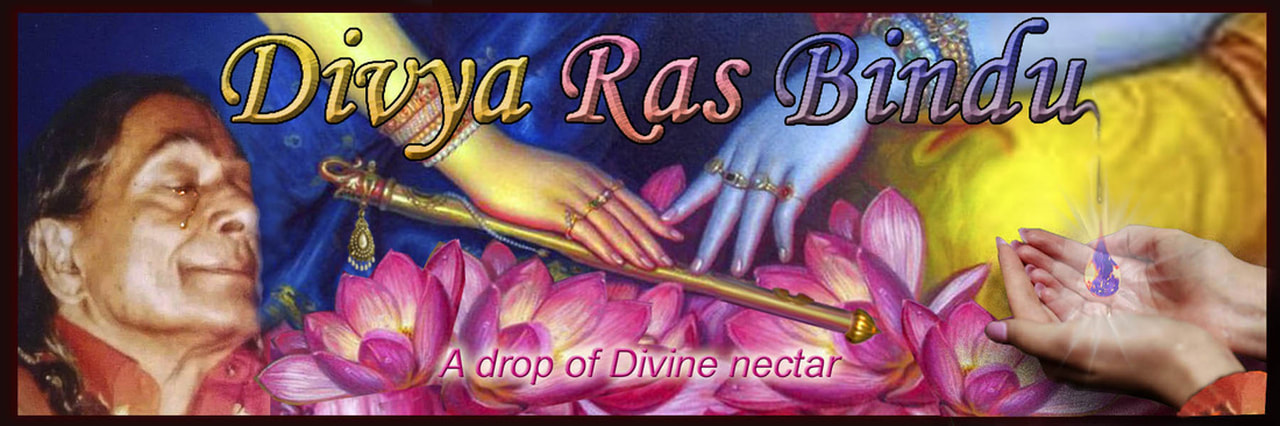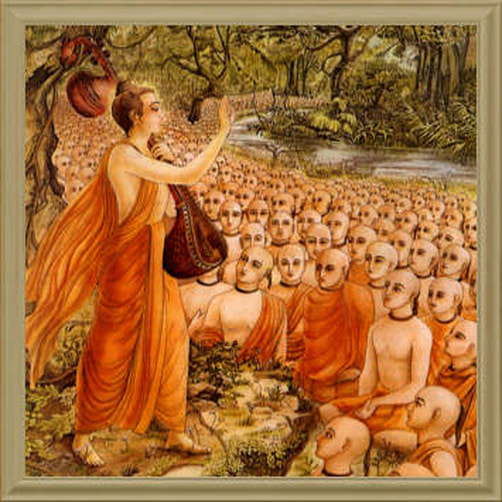|
शास्त्र-वेद में आध्यात्मिक उत्थान के तीन मार्ग हैं -
आइए इन मार्गों की तुलना इन दो मापदंडों के आधार पर करें 1. प्राप्तव्य - इस मार्गावलम्बियों को क्या प्राप्त होता है और 2. कितने समय के लिए प्राप्त होता है । |
Karma
 यदि कोई बिना किसी त्रुटि के वैदिक कर्म करे तो परिणामतः उसको मरणोपरांत सीमित काल के लिये स्वर्ग के सुख प्राप्त होंगे ।
यदि कोई बिना किसी त्रुटि के वैदिक कर्म करे तो परिणामतः उसको मरणोपरांत सीमित काल के लिये स्वर्ग के सुख प्राप्त होंगे ।
कर्म मार्ग का साध्य है स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति (1)।
यदि कोई बिना किसी त्रुटि के वैदिक कर्म करे तो परिणामतः उसको स्वर्ग में सीमित काल के लिये स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जायेंगे । उस सुख को भोगते समय भी मानसिक, दुःख, अतृप्ति, अशान्ति रहेगी । उसके बाद मनुष्य शरीर मिले न मिले । हो सकता है निम्न योनियों में भेज दिया जाए । पुनः मनुष्य रूप प्राप्त होने से पहले करोड़ों कल्प निम्न योनियों में जन्म और मरण का दुःसह दुःख भोगना होगा। केवल मानव शरीर में ही जीव को कर्म करने का अधिकार वापस मिल जाएगा।
तो, कर्म एक सीमित अवधि के लिए स्वर्गीय सुख प्राप्त करने का एक उपकरण या वाहन है। बस । उसके आगे कर्म की गति नहीं है ।
यदि कोई बिना किसी त्रुटि के वैदिक कर्म करे तो परिणामतः उसको स्वर्ग में सीमित काल के लिये स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जायेंगे । उस सुख को भोगते समय भी मानसिक, दुःख, अतृप्ति, अशान्ति रहेगी । उसके बाद मनुष्य शरीर मिले न मिले । हो सकता है निम्न योनियों में भेज दिया जाए । पुनः मनुष्य रूप प्राप्त होने से पहले करोड़ों कल्प निम्न योनियों में जन्म और मरण का दुःसह दुःख भोगना होगा। केवल मानव शरीर में ही जीव को कर्म करने का अधिकार वापस मिल जाएगा।
तो, कर्म एक सीमित अवधि के लिए स्वर्गीय सुख प्राप्त करने का एक उपकरण या वाहन है। बस । उसके आगे कर्म की गति नहीं है ।
Gyan
अब आइए ज्ञान मार्ग पर विचार करें। वेद-शास्त्र कर्म के अतिरिक्त ज्ञान को भी आध्यात्मिक उत्थान का साधन बताते हैं । ज्ञान मार्ग के पथिकों की अंतिम गति अज्ञान का नाश है । माया के जीव पर हावी होने के कारण यह अज्ञान जीव पर हावी हो गया है ।
माया के 2 रूप हैं
1. स्वरूपाविका माया या अविद्या माया - यह माया जीव को अपना वास्तविक स्वरूप भुला देती है । जब यह भूल गया तो धारणा बन गई कि "मैं यह शरीर हूँ"।
2. गुणावरिका माया या विद्या माया - जब ज्ञानी आत्म-ज्ञान प्राप्त करता है तो वह माया के राजस और तामस गुण दब जाते हैं पूर्णतया जाते नहीं हैं । बस दब जाते हैं । फिर भी सत्व गुण प्रमुख रह जाता है।
ज्ञान मार्ग की साधना परिपक्व होने पर साधक स्वरूपावरिका माया से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, आत्मा स्वयं के ज्ञान और आनंद को प्राप्त करती है (आत्मज्ञान) (2)। इस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सभी को आत्मा के रूप में देखता है। इस प्रकार, किसी सांसारिक लाभ में न तो आनंदित होता है न ही सांसारिक हानि के कारण परेशान होता है। इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी सत्त्व गुण प्रबल रहता है। इसलिए, जीव अभी भी गुणवारिका माया के शिकंजे में है इसलिए उसे ब्रह्मज्ञान (निर्गुण निराकार ब्रह्म) का अनुभव नहीं होता है। इतनी ऊँची अवस्था से भी जड़ भरत की भाँति तनिक सी लापरवाही से पतन हो सकता है ।
ऐसे आत्म-ज्ञानी को भगवद्-प्राप्त होने के लिए सगुण-साकार भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। जैसा कि गीता कहती है -
माया के 2 रूप हैं
1. स्वरूपाविका माया या अविद्या माया - यह माया जीव को अपना वास्तविक स्वरूप भुला देती है । जब यह भूल गया तो धारणा बन गई कि "मैं यह शरीर हूँ"।
2. गुणावरिका माया या विद्या माया - जब ज्ञानी आत्म-ज्ञान प्राप्त करता है तो वह माया के राजस और तामस गुण दब जाते हैं पूर्णतया जाते नहीं हैं । बस दब जाते हैं । फिर भी सत्व गुण प्रमुख रह जाता है।
ज्ञान मार्ग की साधना परिपक्व होने पर साधक स्वरूपावरिका माया से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, आत्मा स्वयं के ज्ञान और आनंद को प्राप्त करती है (आत्मज्ञान) (2)। इस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सभी को आत्मा के रूप में देखता है। इस प्रकार, किसी सांसारिक लाभ में न तो आनंदित होता है न ही सांसारिक हानि के कारण परेशान होता है। इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी सत्त्व गुण प्रबल रहता है। इसलिए, जीव अभी भी गुणवारिका माया के शिकंजे में है इसलिए उसे ब्रह्मज्ञान (निर्गुण निराकार ब्रह्म) का अनुभव नहीं होता है। इतनी ऊँची अवस्था से भी जड़ भरत की भाँति तनिक सी लापरवाही से पतन हो सकता है ।
ऐसे आत्म-ज्ञानी को भगवद्-प्राप्त होने के लिए सगुण-साकार भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। जैसा कि गीता कहती है -
भक्त्यामामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ गीता १८.५५
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ गीता १८.५५
जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं
शुद्धयतिनान्तरात्मा कृष्णपदाम्भोजभक्तिमृते ॥
'बिना भक्ति के मन भी शुद्ध नहीं हो सकता'। यह गुणवारिका माया किसी साधन से नहीं जाती । यह भगवद्-कृपा से ही जाती है ।
तो, ज्ञान का अन्तिम लक्ष्य आत्म-ज्ञान और वहाँ से पतन होने का भय ।
तो, ज्ञान का अन्तिम लक्ष्य आत्म-ज्ञान और वहाँ से पतन होने का भय ।
Bhakti
अब हम भक्ति मार्ग की जांच करते हैं।
भक्त्या संजायते भक्त्या
भक्ति का परिणाम भक्ति ही है। साधक मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है, इसी को साधना भक्ति कहते हैं । अभ्यास सिद्धि (परिपक्वता) प्रदान करता है और वह सिद्धा भक्ति कहलाती है, जिसको भगवद्-प्राप्ती भी कहते हैं । दूसरे शब्दों में भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है। भक्ति सदा नित्य वर्धमान (सदा बढ़ने वाली), नित्य-नवायमान (नवीन) है। यहाँ तक कि नारद मुनि, भगवान शंकर और श्रीकृष्ण भी भक्ति ही करते हैं।
फलरूपत्वात्। ना. भ. सू.
अन्य सभी मार्ग ईश्वरप्राप्ति से बहुत पहले ही अपना-अपना फल देने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्ति का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इसके अलावा यह ईश्वर-प्राप्ति के बाद भी बढ़ता है।
भक्ति अजर अमर है (3)। सदातत्व एक असाधारण गुण है और यह गुण केवल भक्ति में ही है।
भक्ति अजर अमर है (3)। सदातत्व एक असाधारण गुण है और यह गुण केवल भक्ति में ही है।